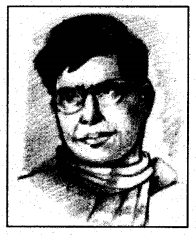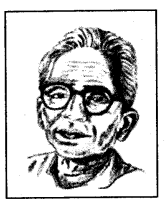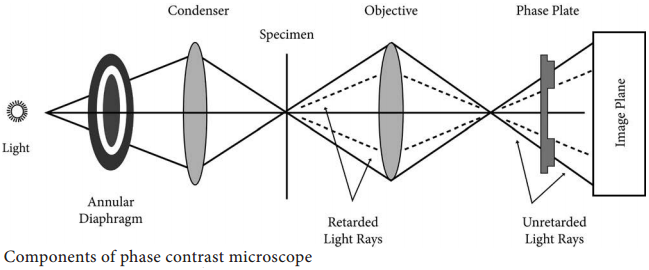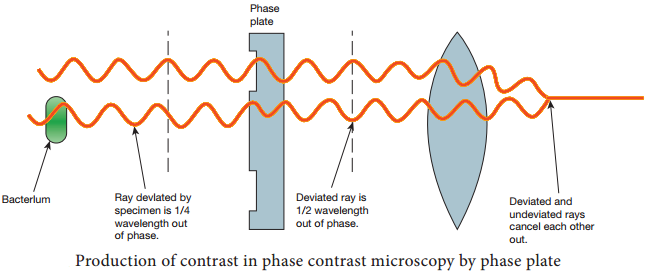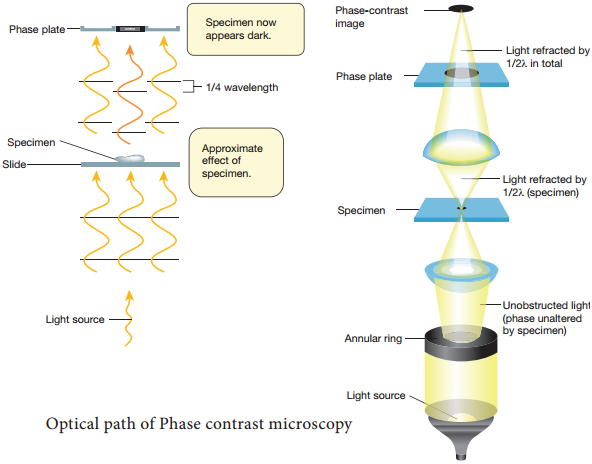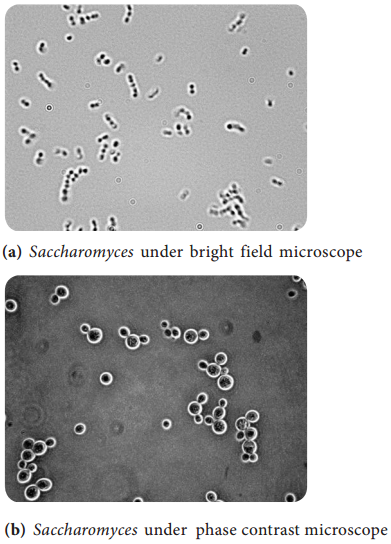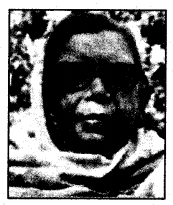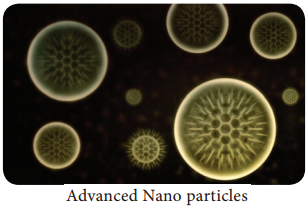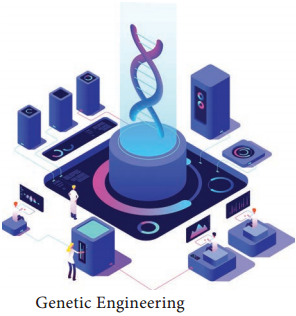By going through these CBSE Class 12 Hindi Notes Chapter 17 शिरीष के फूल Summary, Notes, students can recall all the concepts quickly.
शिरीष के फूल Summary Notes Class 12 Hindi Aroh Chapter 17
शिरीष के फूल पाठ का सारांश
‘शिरीष के फूल’ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित प्रकृति प्रेम से परिपूर्ण निबंध है। इसमें लेखक ने आँधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल फूलों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की जीने की अजेय इच्छा। और कलह-वंद्व के बीच धैर्यपूर्वक लोक-चिंता में लीन कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है।
लेखक जहाँ बैठकर लेख लिख रहा था उसके आगे-पीछे, दाएं-बाएँ शिरीष के फूल थे। अनेक पेड़ जेठ की जलती दोपहर में भी झूम। रहे थे। वे नीचे से ऊपर तक फूलों से लदे हुए थे। बहुत कम ऐसे पेड़ होते हैं जो प्रचंड गर्मी में भी महीनों तक फूलों से लदे रहते हैं। कनेर और अमलतास भी गर्मी में फूलते हैं लेकिन केवल पंद्रह-बीस दिन के लिए। वसंत ऋतु में पलाश का पेड़ भी केवल कुछ दिनों के लिए फूलता है पर फिर से तूंठ हो जाता है। लेखक का मानना है कि ऐसे कुछ देर फूलने वालों से तो न फूलने वाले अच्छे हैं। शिरीष का
पेड़ वसंत के आते ही फूलों से लद जाता है और आषाढ़ तक निश्चित रूप से फूलों से यूँ ही भरा रहता है। कभी-कभी तो भादों मास तक भी फूलता रहता है। भीषण गर्मी में भी शिरीष का पेड़ कालजयी अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ता रहता है। शिरीष के फूल लेखक के हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। पुराने समय में कल्याणकारी और शुभ समझे जाने वाले शिरीष के छायादार पेड़ों को लोग अपनी चारदीवारी के पास लगाना पसंद करते थे। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाम और शिरीष के छायादार हरे-भरे पेड़ निश्चित रूप से बहुत सुंदर लगते हैं। शिरीष की डालियाँ अवश्य कुछ कमजोर होती हैं पर इतनी कमजोर नहीं होती कि उन पर झूले ही न डाले जा सकें। शिरीष के : फूल बहुत कोमल होते हैं। कालिदास का मानना है कि इसके फूल केवल भौंरों के कोमल पैरों का ही दबाव सहन कर सकते हैं। पक्षियों के भार को तो वे बिल्कुल सहन नहीं कर पाते।
इसके फूल चाहे बहुत नर्म होते हैं लेकिन इसके फल बहुत सख्त होते हैं। वे तो साल भर बीत जाने पर भी कभी-कभी पेड़ों पर लटक कर खड़खड़ाते रहते हैं। लेखक का मानना है कि वे उन नेताओं की तरह हैं जो जमाने का दुःख नहीं देखते और जब तक नये लोग उन्हें धक्का मार कर निकाल नहीं देते। लेखक को आश्चर्य होता है कि पुराने की यह अधिकारइच्छा समाप्त क्यों नहीं होती। बुढ़ापा और मृत्यु तो सभी को आना है। शिरीष के फूलों को झड़ना ही होता है पर पता नहीं वे अड़े क्यों रहते हैं ?
वे मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि उन्हें मरना नहीं है। इस संसार में अमर होकर तो कोई नहीं आया। काल देवता की नजर से तो : कोई भी नहीं बच पाता। शिरीष का पेड़ ऐसा है जो सुख-दुःख में सरलता से हार नहीं मानता। जब धरती सूर्य की तेज गर्मी से दहक रही। होती है तब भी वह पता नहीं उससे रस प्राप्त करके किस प्रकार जीवित रहता है। किसी वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया है कि वह वायुमंडल से अपना रस प्राप्त कर लेता है।
लेखक की मान्यता है कि कबीर और कालिदास भी शिरीष की तरह बेपरवाह रहे होंगे क्योंकि जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता वह फक्कड़ नहीं बन सकता। शिरीष के फूल भी फक्कड़पन की मस्ती लेकर झूमते हैं। कालिदास के अभिज्ञानशाकुंतलम् में महाराज दुष्यंत : ने शकुंतला का एक चित्र बनाया पर उन्हें बार-बार यही लगता था कि इसमें कुछ रह गया है। कोई अधूरापन है। काफ़ी देर के बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में वे शिरीष के फूल बनाना तो भूल ही गए थे।
कालिदास की तरह हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर भी कुछ-कुछ अनासक्त थे। शिरीष का पेड़ किसी अवधूत की तरह लेखक के हृदय में तरंगें जगाता है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है। ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं होता। हमारे देश में महात्मा गांधी भी ऐसे ही थे। वह । भी शिरीष की तरह वायुमंडल से रस खींचकर अत्यंत कोमल और अत्यंत कठोर हो गए थे। लेखक जब कभी शिरीष को देखता है उसे ।हृदय से निकलती आवाज सुनाई देती है कि अब वह अवधूत यहाँ नहीं है।
शिरीष के फूल लेखक परिचय
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। उनका जन्म सन् 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था, जो संत स्वभाव के व्यक्ति थे। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में हुई। उन्होंने काशी महाविद्यालय से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात 1930 ई० में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसी वर्ष ये शांतिनिकेतन में हिंदी अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। इसी पद पर रहते हुए इनका रवींद्रनाथ ठाकुर, क्षितिमोहन सेन, आचार्य नंदलाल बसु आदि महानुभावों से संपर्क हुआ।
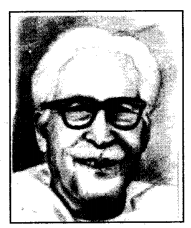
सन् 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सन् 1960 में उनको पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। तत्पश्चात यहाँ से अवकाश लेकर ये भारत सरकार की हिंदी विषयक समितियों एवं योजनाओं से जुड़े रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी० लिट० की मानद उपाधि से अलंकृत किया। ‘आलोक पर्व’ पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने इनकी साहित्य साधना को परखते हए इनको पद्मभूषण की उपाधि से सुशोभित किया। सन् 1979 में दिल्ली में ये अपना उत्कृष्ट साहित्य सौंपकर चिर निद्रा में लीन हो गए।
नार …आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं पर लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं
निबंध-संग्रह-अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज,
विचार-प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद।
उपन्यास-बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा।
आलोचना साहित्येतिहास-हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य : उद्भव और विकास, सूर साहित्य,कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना।
ग्रंथ संपादन-संदेश-रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ-सिदधों की बानियाँ।
पत्रिका-संपादन-विश्वभारती, शांतिनिकेतन। आता माविका पता
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक श्रेष्ठ आलोचक होने के साथ-साथ प्रसिद्ध निबंधकार भी थे। उनका साहित्य कर्म भारत के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। वे एक श्रेष्ठ ललित निबंधकार थे। उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ। निम्नलिखित हैं-
(i) देश-प्रेम की भावना-द्विवेदी जी का साहित्य देश-प्रेम की भावना से ओत-प्रोत है। उनकी मान्यता है कि जिस देश में हम पैदा होते हैं उसके प्रति प्रेम करना हमारा परम धर्म है। उस देश का कण-कण हमारा आत्मीय है। उस मिट्टी के प्रति हमारा अटूट संबंध है। इसलिए इनके साहित्य में अपने देश के प्रति मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक हम अपनी आँखों से अपने देश को देख लेना नहीं सीख लेते तब तक इसके प्रति हमारे मन में सच्चा और स्थायी प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। ‘मेरी जन्मभूमि’ निबंध में उन्होंने लिखा है कि “यह बात अगर छिपाई भी तो कैसे छिप सकेगी कि मैं अपनी जन्मभूमि को प्यार करता हूँ।”
(ii) प्रकृति-प्रेम का चित्रण-द्विवेदी जी के हृदय में प्रकृति के प्रति अपार प्रेम था। उनके निबंध साहित्य में उनका प्रकृति से अनन्य्रेम प्रकट होता है। उन्होंने अपने अनेक निबंधों में प्रकृति के मनोरम और भावपूर्ण चित्र अंकित किए हैं। अशोक के फूल, वसंत आ गया है, नया वर्ष आ गया, शिरीष के फूल आदि में प्रकृति के अनूठे रूप का चित्रण हुआ है। कहीं-कहीं इन्होंने प्रकृति के चेतन रूप का भी अंकन किया है। इनके अनुसार प्रकृति चेतन और भावों से भरी हुई है। इन्होंने प्रकृति के माध्यम से भारतीय
संस्कृति के भी दर्शन किए हैं।
(iii) मानवतावादी दृष्टिकोण-मानवतावादी दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। अनादिकाल से ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ भारतीय संस्कृति का आदर्श रहा है। द्विवेदी जी के निबंधों में मानवतावादी विचारधारा का अनूठा चित्रण मिलता है। इन्होंने अपने निबंधों में मानव कल्याण को प्रमुख स्थान दिया है। इन्होंने मानव-मात्र के कल्याण की कामना की है। इन्होंने मानव को परमात्मा की सर्वोत्तम कृति माना है। उनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु का प्रयोजन मानव कल्याण है। वह मनुष्य को ही साहित्य का लक्ष्य मानते हैं।
(iv) समाज का यथार्थ चित्रण-द्विवेदी जी ने समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने अपने कथा-साहित्य में जाति-पाँति, मजहब के नाम पर बँटे समाज की समस्याओं का वर्णन किया है। वर्षों से पीड़ित नारी संकट को पहचानकर इन्होंने उसका समाधान खोजने का उपाय किया है। इन्होंने स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार माना है तथा उसकी पीड़ा का गहन विश्लेषण करके उसके प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त की है।
(v) भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था-द्विवेदी जी की भारतीय संस्कृति के प्रति गहन आस्था थी। उन्होंने भारत देश को महामानव समुद्र की संज्ञा दी है। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा है। इसे द्विवेदी जी ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण तथा भारतीय संस्कृति की महानता इनके निबंध साहित्य का आधार है। इन्हें संसार के सभी लोगों में मानव संस्कृति के दर्शन होते हैं।
(vi) प्राचीन और नवीन का अद्भुत समन्वय-द्विवेदी जी के निबंध-साहित्य में प्राचीनता और नवीनता का अद्भुत समन्वय है। . उन्होंने प्राचीन ज्ञान, जीवन दर्शन और साहित्य सिद्धांत को नवीन अनुभवों से मिलाकर प्रस्तुत किया है।
(vi) विषय की विविधता-दविवेदी जी ने अनेक विषयों को लेकर अपने निबंधों की रचना की है। उन्होंने ज्योतिष, संस्कृति, प्रकृति, नैतिक, समीक्षात्मक आदि अनेक विषयों को अपनाकर निबंधों की रचना की है।
(viii) ईश्वर में विश्वास-आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते थे। वे एक आस्तिक पुरुष थे। यही भाव उनके निबंधों में भी दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने स्वीकार किया है कि ऐसी कोई परम शक्ति अवश्य है जो इसके पीछे कर्म करती है। उन्होंने माना है कि ईश्वर अनादि, अनंत, अजन्मा, निर्गुण होकर भी अपने प्रभाव को प्रकट करता है। वह इस संसार का जन्मदाता है। लेखक के शब्दों में “इस दृश्यमान सौंदर्य के उस पार इस असमान जगत के अंतराल में कोई एक शाश्वत सत्ता है जो इसे मंगल की ओर ले जाने के लिए कृत निश्चय है।
(ix) भाषा-शैली-द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार थे। उनकी भाषा तत्सम-प्रधान साहित्यिक है। इन्होंने पांडित्य प्रदर्शन को कहीं भी अपने साहित्य में स्थान नहीं दिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में सरल, साधारण, सुबोध और सार्थक शब्दावली का प्रयोग किया है। वे कठिन को भी सरल बनाने में सिद्धहस्त थे। तत्सम शब्दावली के साथ-साथ उन्होंने तद्भव देशज, उर्दू-फ़ारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। हिंदी की गद्य शैली को जो रूप उन्होंने दिया वह हिंदी के लिए वह वरदान है। उन्होंने अपने निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक आदि शैलियों को अपनाया है। वस्तुतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी-साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार थे। उनका निबंध हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि समस्त साहित्य में अपूर्व स्थान है।